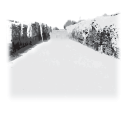शुक्रवार, 23 जनवरी, 1944
मेरी प्यारी किट्टी,
इधर के सप्ताहों मेँ मुझे परिवार के वंश वृक्षोँ और राजसी परिवारों की वंशावली
तालिकाओँ में खासी रूचि हो गई है। मैं इस नतीजे पर पहुँची हूँ कि एक बार तुम खोजना शुरू कर दो तो तुम्हें अतीत मेँ गहरे, और गहरे उतरना पड़ेगा। इस खोज से तुम्हारे हाथ और भी रोचक जानकारियाँ लगेंगी।
हालाँकि जब मेरे स्कूल के काम की बात आती है तो मैं बहुत मेहनत करती हूँ और
रेडियों यर बी.बी.सी. की होम सर्विस को समझ सकती हूँ, इसके बावजूद मैं अपने ज्यादातर रविवार अपने प्रिय फ़िल्मी कलाकारों की तसवीरें अलग करने और देखने में गुज़ारती हूँ। यह संग्रह अच्छा-खासा हो चुका है। मिस्टर कुगलर मुझ पर हर सोमवार कुछ ज्यादा ही मेहरबान
होते है और मेरे लिए सिनेमा एंड थियेटर पत्रिका की प्रति लेते आते हैं। इस घर-परिवार के ऐसे लोग भी ,जो ज़रा भी दुनियादार नहीँ हैँ ,इसे पैसोँ की बरबादी मानते हैँ लेकिन इस बात पर हैरान भी होते हैं कि कैसे मैँ एक साल के बाद भी किसी फ़िल्म के सभी कलाकारों के नाम ऊपर से नीचे तक सही-सही बता सकती हूँ। बेप जो अकसर छुट्टी के दिन अपने बॉयफ्रेंड के साथ फिल्म देखने जाती है, शनिवार को ही मुझे बता देती है कि वे कौन सी फिल्म देखने जा रहे हैँ, तो मैँ फिल्म के मुख्य नायकों और नायिकाओं के नाम तथा समीक्षाएँ
फ़र्राटे से बोलना शुरू कर देती हूँ। हाल ही में मम्मी ने फ़िकरा कसा कि मुझे बाद में फ़िल्में देखने जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योँकि मुझे सारी फिल्मों की कहानियाँ, नायकों के नाम तथा समीक्षाएँ ज़बानी याद हैं।
जब भी मैं नयी केश सज्जा बनाकर बाहर आती हूँ, मैं सबके चेहरों पर उग आई असहमति साफ़-साफ़ पढ़ सकती हूँ। और यह भी बता सकती हूँ कि कोई न कोई ज़रूर टोक देगा कि मैं फलाँ
फिल्म स्टार की नकल कर रही हूँ। मेरा यह जबाब कि ये स्टाइल मेरा खुद का आविष्कार है, मज़ाक के रूप मेँ लिया जाता है। जहाँ तक मेरे हेयर स्टाइल का सवाल है, यह आधे घंटे से ज्यादा नहीं टिका रहता। तब तक मैं उससे बोर ही चुकी होती हूँ और सबकी टिप्पणियाँ सुनते-सुनते मेरे कान पकने लगते हैं। मैं सीधे गुसलखाने की तरफ़ लपकती हूँ और मेरे बाल फिर से पहले की तरह उलझे हुए घुँघराले हो जाते हैं।
तुम्हारी ऐन
बुधवार, 28 जनवरी, 1944
मेरी प्यारी किट्टी,
आज सुबह मैं सोच रही थी कि क्या तुमने अपने आपको
कभी गाय समझा है जिसे हर दिन मेरी बासी खबरें बार-बार चबानी पड़ती हैं। इनकी इतनी अधिक जुगाली कि तुम्हें उबासी आ जाए और तुम मन ही मन कामना करो कि ऐन कुछ नए समाचार दे।
सॉरी, तुम्हें ये नाली के सड़ते पानी की तरह नीरस लगता
होगा। लेकिन ज़रा मेरी हालत की कल्पना करो जिसे रोज़-रोज़ यही सुनना पड़ता है। अगर खाने के वक्त बातचीत राजनीति या अच्छे खाने के बारे मेँ नहीं हो रही होती तो मम्मी या मिसेज़ वान दान
अपने बचपन की उन कहानियों को लेकर बैठ जाती हैं जो हम हज़ार बार सुन चुके हैं या फिर डसेल शुरू हो जाते हैं खूबसूरत रेस के घोड़े ,उनकी चार्लोट का महँगा वॉर्डरोब ,लीक करती नावेँ , चार बरस की उम्र मेँ तैर सकने वाले बच्चे ,दर्द करती माँसपेशियाँ और डरे हुए मरीज़ -ये सब किस्से। इन सारी बातोँ का निचोड़ ये है : जब भी हम आठोँ मेँ से कोई भी अपना मुँह खोलता है , बाकी सातोँ उसके लिए कहानी पूरी कर सकते हैँ। किसी भी लतीफ़े को सुनने से पहले ही हमेँ उसकी पंच लाइन पता होती है । नतीजा यह होता है कि लतीफ़ा सुनाने वाले को अकेले हँसना पड़ता है। अलग-अलग ग्वाले, राशनवाले, कसाई जो घरों की इन दो भूतपूर्व मालकिनों के संपर्क में आए, इतनी बार उनके चरित्र-चित्रण हो चुके हैं कि हमारी कल्पना शक्ति में उनमें जोड़ने के लिए कुछ भी नहीं बचा। एनेक्सी की यह हालत है कि यहाँ नया या ताजा सुनने-सुनाने को कुछ भी नहीं बचा है।
फिर भी, इन सारी चीजों में ताजा सुनने-सुनाने को कुछ भी नहीं बचा है। लोगों को
नमक-मिर्च लगाकर वह सब कुछ दोहराने की आदत न होती जो मिस्टर क्लीमेन, जॉन, मिएप पहले ही बता चुके होते हैं। कई बार मैँ मेज़ के नीचे अपने आपको खुद चिकोटी काट कर रोके रहती हूँ कि कहीं किसी को टोक न दूँ। छोटे बच्चे, खासकर ऐन कभी भी किसी बड़े को टोकने, सही लाइन पर लाने की हिमाकत न करें। भले ही उनकी गाड़ी पटरी से
उतरी जा रही हो या उनकी कल्पनाशक्ति का दिवाला पिट चुका हो।
जॉन और मिस्टर क्लीमेन को अज्ञातवास में छुपे या भूमिगत हो गए लोगों के बारे में बात करना अच्छा लगता है। वे जानते हैं कि हम अपने जैसी हालत में जी रहे लोगों की बातें जानने के इच्छुक हैं। हमें उन सबकी तकलीफ़ोँ से हमदर्दी है जो गिरफ्तार हो गए हैं और उन लोगों की खुशी में हमारी खुशी है जो कैद से आजाद कर दिए गए हैं। भूमिगत होना और अज्ञातवास में चल जाना तो अब आम बात हो गई है । हाँ कई प्रतिरोधी दल भी हैँ ,जैसे फ्री
नीदरलैंड्स जो नकली पहचानपत्र बनाते है, अज्ञातवास में छुपे लोगों को वित्तीय सहायता देते है,
युवा ईसाइयों के लिए काम तलाशते हैं। कितनी हैरानी की बात है कि ये लोग अपनी जान जोखिम में डालकर दूसरों की मदद के लिए कितना काम कर रहे हैं। इसका सबसे बढ़िया
उदाहरण हमारी मदद करने वालोँ का है, जो हमारी आज तक मदद करते आए है और उम्मीद तो यही है कि वे हमें सुरक्षित किनारे तक ले आएँगे। इसका कारण यह है कि अगर वे ऐसा नहीँ करते तो उनकी किस्मत भी हमारी जैसी हो जाएगी । उन्होँने कभी नहीँ कहा कि हम उनके लिए मुसीबत हैँ । वे रोज़ाना ऊपर आते हैँ , पुरूषोँ से कारोबार और राजनीति की बात करते हैँ , महिलाओँ से खाने और युद्ध के समय की मुश्किलोँ की बात करते हैँ , बच्चोँ से किताबोँ और अखबारोँ की बात करते हैँ । हमेशा हर संभव मदद करते हैँ । हमेँ ये बात कभी भी नहीँ भूलनी चाहिए । ऐसे मेँ जब दूसरे लोग जर्मनोँ के खिलाफ़ युद्ध मेँ बाहदुरी दिखा रहे हैँ , हमारे मददगार रोज़ाना अपनी बेहतरीन भावनाओँ और प्यार से हमारा दिल जीत रहे हैँ ।
अजीब-अजीब कहानियाँ चल रही है । उनमें काफ़ी सच भी है । अभी मिस्टर क्लीमेन
गेल्डरलैंड में भूमिगत हो चुके आदमियों और पुलिसवालों के बीच हुए फ़ुटबाल मैच का
ज़िक्र कर रहे थे , हिल्वरसम में नए राशनकार्ड जारी किए गए । (ऐसे लोगों को , जो अज्ञातवास में रह रहे हैँ , राशन खरीदने की सुविधा हो सके ) अगर राशनकार्ड न हो तो एक कार्ड के लिए 60 गिल्डर देने पड़ते हैं। ज़िले मेँ अज्ञातवास मेँ रह रहे सभी लोगों से रजिस्ट्रार ने आग्रह किया कि वे फ़लाँ दिन एक अलग मेज़ पर आकर अपने कार्ड ले जाएँ।
इस सबके साथ ये भी खयाल रखना पड़ता है कि इस तरह
की चालाकियोँ की जर्मनों को हवा भी न लगे।
तुम्हारी ऐन
बुधवार, 29 मार्च, 1944
मेरी प्यारी किट्टी,
कैबिनट मंत्री मिस्टर बोल्के स्टीन ने लंदन से डच प्रसारण मेँ कहा कि युद्ध के बाद युद्ध का वर्णन करने वाली डायरियों और पत्रों का संग्रह किया जाएगा। और फिर हर कोई मेरी डायरी पर
झपट पड़ा। सोचो, ये कितना दिलचस्प होगा जब मैं इस गुप्त एवेक्सी के बारे मेँ छपवाऊँगी। उसका शीर्षक ही ऐसा होगा कि लोग इसे एक जासूसी कहानी समझेंगे।
मैं सही बता रही हूँ, युद्ध के दस साल बाद लोग इससे
कितना चकित होंगे कि जब उन्हेँ पता चलेगा कि हम लोग कैसे रहते थे, हम क्या खाते थे और यहूदियों के रूप मेँ अज्ञातवास मेँ हम क्या-क्या बातें करते थे। हालँकि मैं तुम्हें इस जीवन के बारे मेँ काफी-कुछ बता चुकी हूँ, फिर भी तुम अभी भी थोड़ा-सा ही
जान पाई हो। हवाई हमले के दौरान औरतें कैसी डर जाती हैं; अब देखो ना, पिछले रविवार जब 350 ब्रिटिश वायुयानों ने इज्मुईडेन पर
550 टन गोला-बारूद बरसाया तो हमारे घर ऐसे काँप रहे थे जैसे हवा मेँ घास की पत्तियाँ। या हमारे इन घरों मेँ कैसी महामारियाँ
फैली हुई हैं।
तुम्हें इस सबकी कुछ खबर नहीं है। सब कुछ तुम्हें बताने मेँ पूरा दिन लग जाएगा। लोगों को सब्जियों और सभी प्रकार के सामानों के लिए लाइनों मेँ खड़े होना पड़ता है; डॉक्टर अपने मरीज़ोँ को नहीँ देख पाते ,क्योँकि उन्होँने पीठ मोड़ी नहीँ कि उनकी कारेँ और मोटर साइकिलेँ चुरा ली जाती हैँ ,चोरी -चकारी इतनी बढ़ गई है कि डच लोगोँ मेँ अँगूठी पहनने क रिवाज़ तक नहीँ रह गया है ।
छोटे-छोटे बच्चे आठ-आठ, दस-दस बरस के होंगे लेकिन लोगों के घरों की खिड़कियाँ तोड़ कर घुस जाते हैं और जो भी हाथ लगा, उठा ले जाते हैं। लोग पाँच मिनट के लिए भी अपना घर छोड़ने की हिम्मत नहीं कर सकते हैं, क्योँकि लौटने पर उन्हेँ घर में झाडू फिरी मिलेगी। चोरी गए टाइपराइटरों, ईरानी कालीनों, बिजली से चलने वाली घड़ियों, कपडों आदि को लौटाने के लिए अखबारों में इनाम के विज्ञापन आए दिन पढ़ने को मिलते हैं। गली-गली नुक्कडों पर लगी बिजली से चलने वाली घड़ियाँ लोग उतार ले गए और सार्वजनिक टेलीफ़ोनोँ का पुर्ज़ा-पुर्ज़ा गायब हो चुका है।
डचों की नैतिकता अच्छी नहीं है। सब भूखे हैं ; नकली कॉफ़ी को छोड़ दो तो एक हफ्ते का राशन दो दिन भी नहीं चल पाता। अभी और क्या देखना बाकी है, पुरुषों को जर्मनी
भेजा जा रहा है, बच्चे बीमार हैं या फिर भूख से बेहाल हैं; सब लोग फटे-पुराने कपड़े और घिसे-पिटे जूते पहनकर काम चला रहे हैं। ब्लैक मार्केट में जूते का नया तला 7.50 गिल्डर
का मिलता है। इसके अलावा बहूत कम मोची मरम्मत का काम कर रहे हैं, यदि वे करते
भी हैं तो चार महीने इंतजार करना महंगा और इस बीच जूता गायब हो चुका होगा।
इसका एक लाभ भी हुआ है, खाना जितना खराब होता जा रहा है बिक्री उतनी ही गंभीर
हो रही है; सरकारी लोगों पर हमले की घटनाएँ बढ़ती जा रही हैं। खाद्य कार्यालय, पुलिस, अधिकारी-सभी या तो अपने साथी नागरिकोँ की मदद कर रहे हैँ या उन पर कोई आरोप लगाकर जेल मेँ भेज देते हैँ । सौभाग्य से बहुत कम डच लोग गलत पक्ष मेँ हैँ ।
तुम्हारी ऐन
मंगलवार, 11 अप्रैल, 1944
मेरी प्यारी किट्टी,
मेरा सिर घूम रहा है। समझ में नहीं आ रहा , कहाँ से शुरू करू। गुरुवार (जब मैने
तुम्हें पिछली बार लिखा था) सब कुछ ठीक-ठाक था। शुक्रवार (गुड फ्राइडे) हम मोनापोली खेल खेलते रहे। शनिवार भी हम यही खेल खेले। दिन पता ही नहीं चला, कैसे बीत गए । शनिवार कोई दो बजे का वक्त रहा होगा, तेज़ गोलाबारी शुरू हो गई। मशीनगनें चल रही थीं। मर्द लोगोँ का यही कहना था । बाकी लोगोँ के लिए सब कुछ शांत था ।
रविवार दोपहर के वक्त मेरे आमन्त्रण पर पीटर साढ़े चार बज मुझसे मिलन के लिए
आया। सवा पाँच बजे हम ऊपर सामने वाली अटारी पर चले गए। वहाँ हम छ : बजे तक रहे। छ: बजे से सवा रात बजे तक रेडियों पर बहुत ही खूबसूरत मोत्ज़ार्ट संगीत बज रहा था। मुझे रात्रि राग बहुत ही भले लगे। मैं रसोई में तो संगीत खुन ही नहीं गाती, क्योँकि दिव्य
संगीत मेरी आत्मा की गहराइयों में उतरता चला जाता है। रविवार के दिन पीटर स्नान नहीं कर पाया था। नहाने का टब नीचे ऑफ़िस मेँ गंदे कपडों से भरा हुआ रखा था। हम दोनों ऊपर अटारी पर एक साथ गए। हम दोनों आराम से बैठ सकेँ, इसलिए मुझे जो भी कुशन सामने नज़र आया,
मैं ऊपर लेती गई। हम एक पेटी पर बैठ गए। अब हुआ यह कि एक तो वह पेटी बहुत छोटी थी और दूसरे कुशन भी छोटा-सा ही था, हम दोनों एक-दूसरे से बहुत सट कर बैठे हुए थे। सहारा लेने
के लिए हमारे पीछे दो और पेटियाँ थीँ ही। मोश्ची हमेँ कंपनी देने के लिए हमारे साथ थी ही।
अचानक पौने नौ बजे मिस्टर वान दान ने सीटी बजाई और पूछा कि कहीँ हम मिस्टर डसेल का कुशन तो नहीं ले आए हैं। हम कूदे और कुशन लेकर सीधे नीचे आ गए। बिल्ली और मिस्टर
वान दान हमारे साथ थे। यह कुशन ही सारे झगड़े की जड़ था। डसेल इसलिए खफ़ा थे कि मैं वो तकिया उठा लाई थी जिसे वे कुशन की तरह इस्तेमाल करते थे। उन्हेँ डर था कि उनके तकिए पर पिस्सु
चिपक जाएँगे। उन्होंने सारे घर को सिर पर उठा रखा था क्योँकि हम उनका कुशन उठा लाए थे। बदला लेने की नीयत से पीटर और मैंने उनके बिस्तर मेँ दो कड़े ब्रुश घुसेड़ दिए लेकिन जब मिस्टर डसेल
ने तय किया कि जाकर अपने कमरे मेँ बैठेँगे तो हमें ये ब्रुश निकाल लेने पड़े। इस छोटे से प्रहसन पर हम हँसते-हँसते लोट-पोट हो गए।
लेकिन हमारा हँसी-मज़ाक जल्दी ही खत्म हो गया। साढ़े-नौ बजे पीटर ने हौले से दरवाजा खटखटाया और पापा से कहा कि वे ज़रा ऊपर आएँ, उसे अंग्रेज़ी के एक कठिन वाक्य मेँ दिक्कत आ रही है।
मुझे तो दाल मेँ कुछ काला नज़र आ रहा है। 'मैँने मार्गोट से कहा, 'तय है, पीटर ने किसी और बहाने से यह बात कही है।' जिस तरीके से मर्द लोग बात कर रहे हैं, मैं शर्त लगा कर कह सकती हूँ कि सेंधमारी हो रही थी। पिता जी , मिस्टर वान दान औ रपीटर लपक कर नीचे पहुँच गए । मार्गोट , माँ , मिसेज़ वान दान और मैँ ऊपर इंतज़ार करते रहे । चार डरी-सहमी औरतेँ बातेँ ही तो कर सकती हैँ । जब तक हमने नीचे ज़ोर का एक धमाका नहीँ सुना ,हम बातोँ मेँ लगी रहीँ । उसके बाद का मामला है । मेरा सोचना सही था ।
उसी वक्त गोदाम में सब कुछ शांत हो गया। घड़ी ने पौने दस बजाए। हमारे चेहरों का रंग उड़ चुका था, इसके बावजूद कि हम डरे हुए थे, हम शांत बने रहे। आदमी लोग कहाँ थे? ये धमाके की आवाज कैसी थी ? क्या वे लोग सेंधमारोँ के साथ लड़ रहे थे? हम डर के मारे सोच भी नहीं पा रहे थे । हम सिर्फ़ इंतजार ही कर सकते थे।
दस बजे, सीढ़ियों पर कदमों की आवाजें आई। पापा का चेहरा पीला पड़ चुका था, वे
नर्वस थे। पहले वे भीतर आए। उनके पीछे मिस्टर वान दान, 'बत्तियाँ बंद कर दो, दबे पाँव
ऊपर वाली मंजिल पर चले जाओ, पुलिस के आने की आशंका है।'
अब डरने का वक्त भी नहीं बचा था। बत्तियाँ बुझा दी गईँ थीं। मैने फटाफट एक जैकेट उठाई और हम ऊपर जाकर बैठ गए। हमें कुछ भी बतानेचाला कोई भी नहीं था। मर्द लोग बापस नीचे जा चुके थे। वे चारों दस बज कर दस मिनट तक वापिस ही नहीं आए। दो लोग पीटर की खुली खिड़की में से निगाह रखे हुए थे। सीढियों के बीच वाले दरवाजे पर ताला जड़ दिया गया था। ब्रुककेस बंद कर दिया गया था। हमने रात को जलाई जाने वाली बत्ती
पर एक स्वेटर डाल दिया। तब उन्होंने हमें सब कुछ बताया कि क्या हुआ था।
पीटर अभी सीढ़ियों पर ही था जब उसने ज़ोर के दो धमाके सुने। वह नीचे गया तो
देखता क्या है कि गोदाम के दरवाजे में से बाईं तरफ़ का आधा फट्टा गायब है। वह लपक कर ऊपर आया और 'होम गार्डस' को चौकन्ना किया । वे चारोँ लपके-लपके नीचे गए । जब वे गोदाम मेँ पहुँचे तो सेंधमार अपने धंधे मेँ लगे हुए थे । बिना सोचे-समझे मिस्टर वान दान चिल्लाए,
'पुलिस…' बाहर भागने की आवाजें आईँ। सेँधमार भाग चुके थे । फट्टे को दोबारा
उसकी जगह पर लगाया गया ताकि पुलिस को इस गैप का पता न चले। लेकिन अभी एक
पल भी नहीं बीता था कि फट्टा फिर वापस नीचे गिरा दिया गया । पुरुष लोग...सेँधमारों की ढिठाई पर हैरान थे । मिस्टर वान दान और पीटर गुस्से के मारे थरथराने लगे । मिस्टर वान दान ने दरवाज़े
पर कुल्हाड़ी का एक ज़ोरदार प्रहार किया । उसके बाद सब कुछ शांत हो गया । एक बार फिर फट्टे को उसकी जगह पर जमाया गया और एक बार फिर उनका यह प्रयास निष्फल कर दिया गया । बाहर की तरफ़ से एक आदमी और एक औरत टॉर्च की रोशनी फेंकते दिखाई दिए। 'क्या मुसीबत है... ' उन आदमियों में से एक भुनभुनाया । लेकिन अब संकट यह था कि उनकी भूमिकाएँ बदल चुकी थीं । अब वे पुलिस के बजाए सेंधमारों वाली हालत में आ गए थे । चारों लपक कर ऊपर आए । डसेल और मिस्टर वान दान ने डसेल साहब की किताबेँ उठाईँ ,पीटर ने दरवाज़ा खोला , रसोई तथा प्राइवेट ऑफ़िस की खिड़कियाँ खोलीँ ।फ़ोन को नीचे फ़र्श पर पटका और आखिरकार चारोँ बुककेस के पीछे पहुँचने मेँ सफल हो ही गए ।
तुम्हारी ऐन
मंगलवार, 13 जून, 1944
मेरी प्यारी किट्टी,
मेरा एक और जन्मदिन गुज़र गया है। इस हिसाब से मैं
पंद्रह बरस की ही गई हूँ। मुझे काफ़ी सारे उपहार मिले हैं- स्प्रिँगर की पाँच खंडों वाली कलात्मक इतिहास पुस्तक, चड्ढियोँ का एक सेट, दो बेल्टेँ, एक रूमाल, दही के दो कटोरे, जैम की शीशी,
शहद वाले दो छोटे बिस्किट, मम्मी-पापा की तरफ़ से वनस्पति विज्ञान की एक किताब, मार्गोट की तरफ़ से सोने का एक ब्रेसलेट, वान दान परिवार की तरफ़ से स्टिकर एलबम, डसेल की तरफ़ से बायोमाल्ट और मीठे मटर, मिएप की तरफ़ से मिठाई, बेप की तरफ़ से मिठाई और लिखने के लिए कॉपियाँ और सबसे बड़ी बात मिस्टर कुगलर की तरफ़ से मारिया तेरेसा नाम की किताब तथा क्रीम से भरे
चीज़ के तीन स्लाइस । पीटर ने पीओनी फूलों का खूबसूरत गुलदस्ता दिया। बेचारे को ये उपहार जुटाने मेँ ही अच्छी खासी मेहनत करनी पड़ी। लेकिन वह कुछ और जुटा ही नहीं पाया।
बेहद खराब मौसम-लगातार बारिश, हवाएँ, और उफ़ान पर समुद्र के बावजूद हमले शानदार तरीके से जारी हैं।
कल चर्चिल, स्मट्स, आइज़नहावर, तथा आर्मोल्ड उन फ्रांसीसी गाँवोँ मेँ गए जिन पर ब्रिटिश सैनिकों ने पहले कब्जा कर लिया था
और बाद मेँ मुक्त कर दिया। चर्चिल एक टॉरपीडो नाव मेँ थे। इससे तटों पर गोलाबारी की जाती है। बहुत से लोगों की तरह चर्चिल को भी पता नहीं है-डर किस चिड़िया का नाम है। जन्मजात बहादुर ।
यहाँ हमारी एनेक्सी की किलेबंदी से डच लोगों के मूड की थाह पाना बहुत मुश्किल है । इस बात मेँ कोई शक नहीँ कि लोगबाग बैठे ठाले भी खुश रह लेते हैँ । ब्रिटिश सैनिकोँ ने आखिर अपनी कमर कस ही ली है और अपने मकसद को पूरा करने के लिए निकल पड़े हैँ । जो लोग ये दावे करते फिर रहे हैँ कि वे ब्रिटिश द्वारा कब्ज़ा किए जाने के पक्ष मेँ नहीँ हैँ , नहीँ जानते कि वे कितनी गलती पर हैँ । उनके तर्क का कारण इतना भर है -ब्रिटिश को लड़ते रहना चाहिए ,संघर्ष करना चाहिए ,और हॉलैँड को आज़ाद कराने के लिए अपने शूरवीर सैनिकों की शहादत के लिए आगे आना चाहिए। हॉलैंड के साथ-साथ कब्जे वाले दूसरे देशों को भी आजाद कराना चाहिए, लेकिन उसके बाद ब्रिटिश को हॉलैंड में रुकना नहीं चाहिए। इसके बजाय उन्हेँ चाहिए कि वे सभी कब्ज़े वाले देशों से हाथ जोड़-जोड़कर माफी माँगें, डच ईस्ट इंडीज को उसके सही हकदारों के हाथोँ में सौंपे और थके, टूटे, हारे और लुटे-पिटे अपने देश ब्रिटेन में लौट जाएँ। मूर्खोँ की कहीं कोई कमी नहीं है। इसके बावजूद, जैसा कि मैने कहा, कुछेक समझदार डच लोगों की भी कमी नहीं है। अगर ब्रिटिश ने जर्मनी के साथ शांति संधि पर हस्ताक्षर कर लिए होते तो हॉलैंड और उसके पड़ोसी देशों का क्या हाल हुआ होता। उसके पास ऐसा करने के बहुत मौके मौजूद थे। हॉलैँड जर्मनी बन चुका होता और तब-यह होना ही समाप्ति का संकेत होता। सब कुछ खत्म हो जाने का संकेत ।
ऐसे सभी डच लोग, जो अभी भी ब्रिटिश को हिकारत से देखते हैं, ब्रिटेन की खिल्ली
उड़ाते हैं, उसके बुढ़ाते लॉर्डोँ की सरकार को ताने मारते हैं, उन्हें कायर कहते हैं, इसके बावजूद जर्मनों से नफ़रत करते हैं, एक अच्छा-खासा सिखाने के लायक हैँ । उनकी जमकर मरम्त की जानी चाहिए तभी हमारे जंग लगे दिमाग खुलेँगे । उनमेँ जोश आएगा ।
मेरे दिमाग में हर समय इच्छाएँ, विचार, आरोप तथा डाँट-फटकार ही चक्कर खाते रहते हैं। मैं सचमुच उतनी घमंडी नहीं हूँ जितना लोग मुझे समझते हैं। मैँ किसी और की तुलना में अपनी कई कमजोरियों और खामियों को बेहतर तरीके से जानती हूँ। लेकिन एक फ़र्क है-मैँ जानती हूँ कि मैँ खुद को बदलना चाहती हूँ, बदलूँगी और काफ़ी हद तक बदल चुकी हूँ।
तब ऐसा क्यों है, मैं अपने आप से यह सवाल पूछती हूँ कि लोग मुझे अभी भी इतना
नाक घुसेड़ू और अपने आपकी तीसमारखाँ समझने वाली क्यों मानते हैं? क्या मैँ वाकई
अक्खड़ हूँ ? क्या मैँ ही अकेली अक्खड़ हूँ या वे सब ही हैं? यह सब वाहियात लगता है, मुझे पता है। लेकिन मैं ऊपर लिखा ये आखिरी वाक्य काटने वाली नहीं। ये वाक्य इतना
मूर्खतापूर्ण नहीं है जितना लगता है। मुझ पर हमेशा आरोपों की बौछार करते रहने वाले दो लोग है मिसेज वान दान और डसेल, उनके बारे में सबको पता है कि वे कितने जड़बुद्धि हैँ । मूर्ख जिसके आगे कोई विशेषण लगाने की ज़रूरत नहीँ । मूर्ख लोग आमतौर पर इस बात को सहन नहीँ कर पाते कि कोई उनसे बेहतर काम करके दिखाए । और इसका सबसे बढ़िया उदाहरण ये दो ज़ड़मति, मिसेज़ वान दान और मूर्खाधिराज डसेल हैँ। मिसेज़ वान दान मुझे
इसलिए मूर्ख समझती हैँ क्योँकि मैं उनके जितनी बीमारियों की शिकार नहीं हूँ। वे मुझे अक्खड़ समझती है क्योँकि वे मुझसे भी ज्यादा अक्खड़ हैं। वे समझती है कि मेरी पोशाकेँ छोटी पड़ गई हैं, क्योंकि उनकी पोशाकें और भी ज्यादा छोटी पड़ गई हैं। और वे समझती कि मैं अपने अपाको कुछ ज्यादा ही तीसमारखाँ समझती हूँ क्योँकि वे उन विषयों पर मुझसे भी दो गुना ज्यादा बोलती हैं जिनके बारे मेँ वे खाक भी नहीं जानतीं। यह बात डसेल पर भी फिट होती है। लेकिन मेरी प्रिय
कहावत है-"जहाँ आग होगी, धुआँ भी वहीं होगा'। और मुझे यह मानने मेँ रत्ती-भर भी संकोच नहीं है कि मैं सब कुछ जानती हूँ।
मेरे व्यक्तित्व के साथ सबसे मुश्किल बात यह है कि मैं
किसी भी और व्यक्ति की तुलना मेँ अपने आपको सबसे
धिक्कारती हूँ , यदि माँ अपनी सलाहें देना शुरू कर देती हैं तो उनके उपदेशों की पोटली इतनी भारी हो जाती है कि मुझे डर लगने लगता है- कैसे होगी इससे मुक्ति! जब तक ऐन का वही पुराना रूप सामने नहीं आ जाता-'मुझे कोई नहीं समझता।'
यह वाक्य मेरा हिस्सा है। बेशक लगे कि ऐसा नहीं होगा,
फिर भी इसमें थोड़े से सच का अंश है। कई बार तो मैं अपने
आपको प्रताडित करते हुए इतनी गहरे उतर जाती हूँ कि सांत्वना के दो बोल सुनने के लिए तरस जाती हूँ कि कोई आए और मुझे इससे उबारे। काश, कोई तो होता जो मेरी भावनाओँ को गंभीरता से समझ पाता। अफ़सोस, ऐसा व्यक्ति मुझे अब तक नहीं मिला है, इसलिए तलाश जारी रहेगी।
मुझे पता है, तुम पीटर के बारे मेँ सोचकर हैरान हो रही ही। नहीं क्या, किट्टी? मैं मानती हूँ कि यह सच है कि पीटर मुझे प्यार करता है गर्लफ्रेंड की तरह नहीं बल्कि एक दोस्त की तरह । उसका स्नेह दिन पर दिन बढ़ता ही जा रहा है; लेकिन कई बार
कोई रहस्यमयी ताकत हम दोनों को पीछे की तरफ़ खींचती है। मैं नहीं जानती कि वो कौन-सी शक्ति है।
कई बार मैं सोचती हूँ कि मैं उसके पीछे जिस तरह
प्रेमदीवानी बनी रहती हूँ, उसे बढ़ा-चढ़ाकर बता रही हूँ, लेकिन यह सच नहीं है। इसका कारण यह है कि अगर मैं उसके कमरे मेँ एक-दो दिन के लिए न जा पाऊं तो मेरी बुरी हालत हो जाती है। मैं उसके लिए तड़पऩे लगती हूँ। पीटर अच्छा और भला लड़का है ; लेकिन उसने मुझे कई तरह से निराश किया है । धर्म के प्रति उसकी नफ़रत ,खाने के बारे मेँ उसका बातेँ करना और इस तरह की और कई बातेँ मैँ बिलकुल भी पसंद नहीँ करती । इसके बावजूद मुझे पक्का यकीन है कि हमने जो वायदा किया है कि कभी झगड़ेगे नहीं, हम उस
पर हमेशा टिके रहेंगे। पीटर शांतिप्रिय, सहनशील और बेहद सहज आत्मीय व्यक्ति है। वह मुझे कई ऐसी बातें भी कह लेने देता है जिन्हेँ कहने की वह अपनी मम्मी को भी इजाज़त न देता। वह दृढ निश्चयी होकर इस मुहिम पर जुटा हुआ है कि वह अपने पर लगे हुए सभी इल्ज़ामों से अपने आपको पाक-साफ़ करें और अपने काम-काज़ में सलीका लाए। इसके बावजूद वह अपने भीतरी 'स्व' को मुझसे छुपाता क्योँ है और मुझे कभी भी इस बात की अनुमति नहीं देता कि मैँ उसमें झाँकूँ। निश्चय ही, वह मेरी तुलना में ज्यादा घुन्ना है, लेकिन
मैँ अनुभव से जानती हूँ (हालँकि मुझ पर लगातार यह आरोप लगाया जाता है कि जो कुछ भी जानना चाहिए वह मैँ थ्योरी में जानती हूँ, व्यवहार में नहीं) कि कई बार, ऐसे घुन्ने लोग भी, जिनसे संवाद कर पाना बहूत मुश्किल होता है, अपनी बात किसी से कह पाने की उत्कट चाह लिए होते हैं।
पीटर और मैँने, दोनों ने अपने चिंतनशील बस्स, एनेक्सी में ही बिताए हैं। हम अकसर
भविष्य, वर्तमान और अतीत की बातें करते हैं, लेकिन जैसा कि मैं तुम्हें बता चुकी हूँ, मैँ
असली चीज की कमी महसूस करती हूँ और जानती हूँ कि वह मौजूद है।
क्या इसका कारण यह है कि मैँ अरसे से बाहर नहीं निकली हूँ और प्रकृति के लिए
पागल हुई जा रही हूँ। मैं उस वक्त को याद करती हूँ जब नीला आसमान , पक्षियोँ की चहचहाने की आवाज़ , चाँदनी और खिलती कलियाँ ,इन चीज़ोँ ने मुझे कभी भी अपने जादू से बाँधा न होता। मेरे यहाँ आने के बाद चीज़ेँ बदल गई हैं। उदाहरण के लिए छुट्टियों के दौरान की बात है। बेहद गरमी थी। मैं रात के साढ़े ग्यारह बजे तक जबरदस्ती आँखें खोले बैठी रही ताकि मैं अपने अकेले के बूते पर अच्छी तरह चाँद को देख सकूँ । अफ़सोस, मेरी
सारी मेहनत बेकार गई। चौंध इतनी ज्यादा थी कि खिड़की खेलने का जोखिम नहीं लिया जा सकता था। कई महीने बाद एक और मौका ऐसा आया था। उस रात मैं ऊपर वाली मंजिल पर थी। खिड़की खुली हुई थी। जब तक खिड़की बंद करने का वक्त नहीं हो गया है मैँ वहीं बैठी रही। यह गहरी, साँवली बरसात की रात थी। तेज हवाएँ चल रही थीं। बादलों के बीच लुकाछिपी चल रही थी। इस सारे नज़ारे ने मुझे मंत्रमुग्ध कर दिया था। पिछले डेढ़ बरस में पहली बार हो रहा था कि मैँ आमने-सामने रात से साक्षात्कार कर रही थी। उम शाम के बाद प्रकृति से साक्षात्कार करने की मेरी चाह लगातार बढ़ती गई थी । तब मुझे चोर उचक्कोँ , मोटे काले चूहे या पुलिस के छापे का भी डर नहीँ रहा था । मैं अकेले ही नीचे चली गई थी और रसोई तथा प्राइवेट ऑफ़िस की खिड़की से प्रकृति के नज़ारे देखती रही
थी । कई लोग सोचते हैँ कि प्रकृति सुंदर होती है, कई लोग समय-समय पर तारों भरे
आसमान के तले सोते हैं,और कई लोग अस्पतालों और जेलों में उस दिन की राह देखते रहते हैं कि वे कब आजाद होंगे और वे फिर से प्रकृति के इस अनूठे उपहार का आनंद ले पाएँगे। प्रकृति गरीब-अमीर के बीच कोई भेदभाव नहीं करती।
यह मेरी कल्पना मात्र नहीं है-आसमान, बादलों, चाँद और
तारों की तरफ़ देखना मुझे शांति और आशा की भावना से सराबोर कर देता है। यह वेलेरियन या ब्रोमाइड की तुलना मेँ आजमाया हुआ
बेहतर नुस्खा है। शांति पाने की रामबाण दबा। प्रकृति मुझे विनम्रता का उपहार देती है और इससे मैं बड़े से बड़ा धक्का भी हिम्मत के साथ झेल जाती हूँ। लेकिन किस्मत का लिखा यही है-कुछेक दुर्लभ अवसरों को छोड़कर मैं मैल से चीकट हुई खिड़कियोँ मेँ खुँसे गंदे परदों मेँ से प्रकृति को बहुत ही कम निहार पाती हूँ। इस तरह से देखने से आनंद लेने की सारी भावना ही मर जाती है। प्रकृति ही तो एक ऐसा वरदान है जिसका कोई सानी नहीं।
कई प्रश्नों मेँ से एक प्रश्न जो मुझे अकसर परेशान करता
रहता है और अभी भी समझा जाता है यह कह देना वहुत ही आसान है कि ये गलत है, लेकिन मेरे लिए इतना ही काफ़ी नहीं है। मैं इस
विराट अन्याय के कारण जानना चाहती हूँ।
संभवत: पुरुषों ने औरतों पर शुरू से ही इस आधार पर शासन करना शुरू किया कि वे उनकी तुलना मेँ शारीरिक रूप से ज्यादा सक्षम हैं; पुरुष ही कमाकर लाता है; बच्चे पालता पोसता है; और जो मन मेँ आए, करता है, लेकिन हाल ही मेँ स्थिति बदली है।
औरतें अब तक इन सबको सहती चली आ रही थीं, जो कि बेवकूफ़ी ही थी। चूँकि इस प्रथा को जितना अधिक जारी रखा गया, यह उतनी ही गहराई से अपनी जड़ेँ जमाती चली गई । सौभाग्य से , शिक्षा ,काम तथा प्रगति ने औरतोँ की आँखेँ खोली हैँ । कई देशोँ मेँ तो उन्हेँ बराबरी का हक दिया जाने लगा है । कई लोगोँ ने कई औरतोँ ने और कुछेक पुरुषोँ ने भी अब इस बात को महसूस किया है कि इतने लंबे अरसे तक इस तरह की वाहियात स्थिति को झेलते जाना गलत ही था । आधुनिक महिलाएँ पूरी तरह स्वतंत्र होने का हक चाहती हैँ ।
लेकिन इतना ही काफ़ी नहीं है। महिलाओँ का भी पूरा सम्मान किया जाना चाहिए।
आमतौर पर देखा जाए तो पूरी दुनिया में पुरुष वर्ग को पूरा सम्मान मिलता है तो महिलाओँ ने ही क्या कुसूर किया है कि वे इससे वंचित रहेँ और उन्हेँ अपने हिस्से का सम्मान न मिले। सैनिकों और युद्धों के वीरों का सम्मान किया जाता है, उन्हेँ अलंकृत किया जाता है, उन्हेँ अमर बना डालने तक का शौर्य प्रदान किया जाता है, शहीदों को पूजा भी जाता है, लेकिन
कितने लोग ऐसे हैं जो औरतों को भी सैनिक का दर्जा देते हैं?
'मौत के खिलाफ़ मनुष्य' नाम की किताब में मैंने पढ़ा था कि आमतौर पर युद्ध में लड़ने वाले वीर को जितनी तकलीफ़, पीड़ा, बीमारी और यंत्रणा से गुज़रना पड़ता है, उससे कहीं अधिक तकलीफ़ेँ औरतें बच्चे को जन्म देते समय झेलती हैं और इन सारी तकलीफ़ोँ से गुज़रने के बाद उसे पुरस्कार क्या मिलता है? जब बच्चा जनने के बाद उसका शरीर अपना आकर्षण खो देता है तो उसे एक तरफ़ धकिया दिया जाता है, उसके बच्चे उसे छोड़
देते हैं और उसका सौँदर्य उससे विदा ले लेता है। औरत ही तो है जो मानव जाति की
निरंतरता को बनाए रखने के लिए इतनी तकलीफ़ोँ से गुज़रती है और संघर्ष करती है, बहुत अधिक मज़बूत और बहादुर सिपाहियों से भी ज्यादा मेहनत करके खटती है। वह जितना संघर्ष करती है, उतना तो बड़ी-बड़ी डीँगेँ हाँकनेवाले ये सारे सिपाही मिलकर भी नही करते ।
मेरा ये कहने का कतई मतलब नहीं है कि औरतों को बच्चे जनना बंद कर देना चाहिए , इसके विपरीत प्रकृति चाहती है कि वे ऐसा करें और इस वजह से उन्हेँ यह काम करते रहना चाहिए। मैं जिस चीज की भर्त्सना करती हूँ वह है हमारे मूल्यों की प्रथा और ऐसे व्यक्तियों की मैँ भर्त्सना करती हूँ जो यह बात मानने को तैयार ही नहीं होते कि समाज में औरतों, खूबसूरत और सौँदर्यमयी औरतों का योगदान कितना महान और मुश्किल है।
मैं इस पुस्तक के लेखक श्री पोल दे क्रुइफ जी से पूरी तरह सहमत हूँ जब वे कहते है कि पुरुषों को यह बात सीखनी ही चाहिए कि संसार के जिन हिस्सों को हम सभ्य कहते
हैं-वहाँ जन्म अनिवार्य और टाला न जा सकने वाला काम नहीं रह गया है। आदमियों के
लिए बात करना वहुत आसान होता है-उन्हेँ औरतों द्वारा झेली जाने वाली तकलीफ़ो से कभी भी गुजरना नहीं पड़ेगा।
मेरा विश्वास है कि अगली सदी आने तक यह मान्यता बदल चुकी होगी कि बच्चे पैदा करना ही औरतोँ का काम है । औरतेँ ज़्यादा सम्मान और सराहना की हकदार बनेँगी ।वे सब औरतेँ जो एक उफ़ भी किए बिना ,यह लंबे-चौड़े बखानोँ के बिना ये तकलीफ़ेँ सहती हैँ ।
तुम्हारी
ऐन.एम.फ्रैँक
-अनुवाद : सूरज प्रकाश
मेरी प्यारी किट्टी,
इधर के सप्ताहों मेँ मुझे परिवार के वंश वृक्षोँ और राजसी परिवारों की वंशावली
तालिकाओँ में खासी रूचि हो गई है। मैं इस नतीजे पर पहुँची हूँ कि एक बार तुम खोजना शुरू कर दो तो तुम्हें अतीत मेँ गहरे, और गहरे उतरना पड़ेगा। इस खोज से तुम्हारे हाथ और भी रोचक जानकारियाँ लगेंगी।
हालाँकि जब मेरे स्कूल के काम की बात आती है तो मैं बहुत मेहनत करती हूँ और
रेडियों यर बी.बी.सी. की होम सर्विस को समझ सकती हूँ, इसके बावजूद मैं अपने ज्यादातर रविवार अपने प्रिय फ़िल्मी कलाकारों की तसवीरें अलग करने और देखने में गुज़ारती हूँ। यह संग्रह अच्छा-खासा हो चुका है। मिस्टर कुगलर मुझ पर हर सोमवार कुछ ज्यादा ही मेहरबान
होते है और मेरे लिए सिनेमा एंड थियेटर पत्रिका की प्रति लेते आते हैं। इस घर-परिवार के ऐसे लोग भी ,जो ज़रा भी दुनियादार नहीँ हैँ ,इसे पैसोँ की बरबादी मानते हैँ लेकिन इस बात पर हैरान भी होते हैं कि कैसे मैँ एक साल के बाद भी किसी फ़िल्म के सभी कलाकारों के नाम ऊपर से नीचे तक सही-सही बता सकती हूँ। बेप जो अकसर छुट्टी के दिन अपने बॉयफ्रेंड के साथ फिल्म देखने जाती है, शनिवार को ही मुझे बता देती है कि वे कौन सी फिल्म देखने जा रहे हैँ, तो मैँ फिल्म के मुख्य नायकों और नायिकाओं के नाम तथा समीक्षाएँ
फ़र्राटे से बोलना शुरू कर देती हूँ। हाल ही में मम्मी ने फ़िकरा कसा कि मुझे बाद में फ़िल्में देखने जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योँकि मुझे सारी फिल्मों की कहानियाँ, नायकों के नाम तथा समीक्षाएँ ज़बानी याद हैं।
जब भी मैं नयी केश सज्जा बनाकर बाहर आती हूँ, मैं सबके चेहरों पर उग आई असहमति साफ़-साफ़ पढ़ सकती हूँ। और यह भी बता सकती हूँ कि कोई न कोई ज़रूर टोक देगा कि मैं फलाँ
फिल्म स्टार की नकल कर रही हूँ। मेरा यह जबाब कि ये स्टाइल मेरा खुद का आविष्कार है, मज़ाक के रूप मेँ लिया जाता है। जहाँ तक मेरे हेयर स्टाइल का सवाल है, यह आधे घंटे से ज्यादा नहीं टिका रहता। तब तक मैं उससे बोर ही चुकी होती हूँ और सबकी टिप्पणियाँ सुनते-सुनते मेरे कान पकने लगते हैं। मैं सीधे गुसलखाने की तरफ़ लपकती हूँ और मेरे बाल फिर से पहले की तरह उलझे हुए घुँघराले हो जाते हैं।
तुम्हारी ऐन
बुधवार, 28 जनवरी, 1944
मेरी प्यारी किट्टी,
आज सुबह मैं सोच रही थी कि क्या तुमने अपने आपको
कभी गाय समझा है जिसे हर दिन मेरी बासी खबरें बार-बार चबानी पड़ती हैं। इनकी इतनी अधिक जुगाली कि तुम्हें उबासी आ जाए और तुम मन ही मन कामना करो कि ऐन कुछ नए समाचार दे।
सॉरी, तुम्हें ये नाली के सड़ते पानी की तरह नीरस लगता
होगा। लेकिन ज़रा मेरी हालत की कल्पना करो जिसे रोज़-रोज़ यही सुनना पड़ता है। अगर खाने के वक्त बातचीत राजनीति या अच्छे खाने के बारे मेँ नहीं हो रही होती तो मम्मी या मिसेज़ वान दान
अपने बचपन की उन कहानियों को लेकर बैठ जाती हैं जो हम हज़ार बार सुन चुके हैं या फिर डसेल शुरू हो जाते हैं खूबसूरत रेस के घोड़े ,उनकी चार्लोट का महँगा वॉर्डरोब ,लीक करती नावेँ , चार बरस की उम्र मेँ तैर सकने वाले बच्चे ,दर्द करती माँसपेशियाँ और डरे हुए मरीज़ -ये सब किस्से। इन सारी बातोँ का निचोड़ ये है : जब भी हम आठोँ मेँ से कोई भी अपना मुँह खोलता है , बाकी सातोँ उसके लिए कहानी पूरी कर सकते हैँ। किसी भी लतीफ़े को सुनने से पहले ही हमेँ उसकी पंच लाइन पता होती है । नतीजा यह होता है कि लतीफ़ा सुनाने वाले को अकेले हँसना पड़ता है। अलग-अलग ग्वाले, राशनवाले, कसाई जो घरों की इन दो भूतपूर्व मालकिनों के संपर्क में आए, इतनी बार उनके चरित्र-चित्रण हो चुके हैं कि हमारी कल्पना शक्ति में उनमें जोड़ने के लिए कुछ भी नहीं बचा। एनेक्सी की यह हालत है कि यहाँ नया या ताजा सुनने-सुनाने को कुछ भी नहीं बचा है।
फिर भी, इन सारी चीजों में ताजा सुनने-सुनाने को कुछ भी नहीं बचा है। लोगों को
नमक-मिर्च लगाकर वह सब कुछ दोहराने की आदत न होती जो मिस्टर क्लीमेन, जॉन, मिएप पहले ही बता चुके होते हैं। कई बार मैँ मेज़ के नीचे अपने आपको खुद चिकोटी काट कर रोके रहती हूँ कि कहीं किसी को टोक न दूँ। छोटे बच्चे, खासकर ऐन कभी भी किसी बड़े को टोकने, सही लाइन पर लाने की हिमाकत न करें। भले ही उनकी गाड़ी पटरी से
उतरी जा रही हो या उनकी कल्पनाशक्ति का दिवाला पिट चुका हो।
जॉन और मिस्टर क्लीमेन को अज्ञातवास में छुपे या भूमिगत हो गए लोगों के बारे में बात करना अच्छा लगता है। वे जानते हैं कि हम अपने जैसी हालत में जी रहे लोगों की बातें जानने के इच्छुक हैं। हमें उन सबकी तकलीफ़ोँ से हमदर्दी है जो गिरफ्तार हो गए हैं और उन लोगों की खुशी में हमारी खुशी है जो कैद से आजाद कर दिए गए हैं। भूमिगत होना और अज्ञातवास में चल जाना तो अब आम बात हो गई है । हाँ कई प्रतिरोधी दल भी हैँ ,जैसे फ्री
नीदरलैंड्स जो नकली पहचानपत्र बनाते है, अज्ञातवास में छुपे लोगों को वित्तीय सहायता देते है,
युवा ईसाइयों के लिए काम तलाशते हैं। कितनी हैरानी की बात है कि ये लोग अपनी जान जोखिम में डालकर दूसरों की मदद के लिए कितना काम कर रहे हैं। इसका सबसे बढ़िया
उदाहरण हमारी मदद करने वालोँ का है, जो हमारी आज तक मदद करते आए है और उम्मीद तो यही है कि वे हमें सुरक्षित किनारे तक ले आएँगे। इसका कारण यह है कि अगर वे ऐसा नहीँ करते तो उनकी किस्मत भी हमारी जैसी हो जाएगी । उन्होँने कभी नहीँ कहा कि हम उनके लिए मुसीबत हैँ । वे रोज़ाना ऊपर आते हैँ , पुरूषोँ से कारोबार और राजनीति की बात करते हैँ , महिलाओँ से खाने और युद्ध के समय की मुश्किलोँ की बात करते हैँ , बच्चोँ से किताबोँ और अखबारोँ की बात करते हैँ । हमेशा हर संभव मदद करते हैँ । हमेँ ये बात कभी भी नहीँ भूलनी चाहिए । ऐसे मेँ जब दूसरे लोग जर्मनोँ के खिलाफ़ युद्ध मेँ बाहदुरी दिखा रहे हैँ , हमारे मददगार रोज़ाना अपनी बेहतरीन भावनाओँ और प्यार से हमारा दिल जीत रहे हैँ ।
अजीब-अजीब कहानियाँ चल रही है । उनमें काफ़ी सच भी है । अभी मिस्टर क्लीमेन
गेल्डरलैंड में भूमिगत हो चुके आदमियों और पुलिसवालों के बीच हुए फ़ुटबाल मैच का
ज़िक्र कर रहे थे , हिल्वरसम में नए राशनकार्ड जारी किए गए । (ऐसे लोगों को , जो अज्ञातवास में रह रहे हैँ , राशन खरीदने की सुविधा हो सके ) अगर राशनकार्ड न हो तो एक कार्ड के लिए 60 गिल्डर देने पड़ते हैं। ज़िले मेँ अज्ञातवास मेँ रह रहे सभी लोगों से रजिस्ट्रार ने आग्रह किया कि वे फ़लाँ दिन एक अलग मेज़ पर आकर अपने कार्ड ले जाएँ।
इस सबके साथ ये भी खयाल रखना पड़ता है कि इस तरह
की चालाकियोँ की जर्मनों को हवा भी न लगे।
तुम्हारी ऐन
बुधवार, 29 मार्च, 1944
मेरी प्यारी किट्टी,
कैबिनट मंत्री मिस्टर बोल्के स्टीन ने लंदन से डच प्रसारण मेँ कहा कि युद्ध के बाद युद्ध का वर्णन करने वाली डायरियों और पत्रों का संग्रह किया जाएगा। और फिर हर कोई मेरी डायरी पर
झपट पड़ा। सोचो, ये कितना दिलचस्प होगा जब मैं इस गुप्त एवेक्सी के बारे मेँ छपवाऊँगी। उसका शीर्षक ही ऐसा होगा कि लोग इसे एक जासूसी कहानी समझेंगे।
मैं सही बता रही हूँ, युद्ध के दस साल बाद लोग इससे
कितना चकित होंगे कि जब उन्हेँ पता चलेगा कि हम लोग कैसे रहते थे, हम क्या खाते थे और यहूदियों के रूप मेँ अज्ञातवास मेँ हम क्या-क्या बातें करते थे। हालँकि मैं तुम्हें इस जीवन के बारे मेँ काफी-कुछ बता चुकी हूँ, फिर भी तुम अभी भी थोड़ा-सा ही
जान पाई हो। हवाई हमले के दौरान औरतें कैसी डर जाती हैं; अब देखो ना, पिछले रविवार जब 350 ब्रिटिश वायुयानों ने इज्मुईडेन पर
550 टन गोला-बारूद बरसाया तो हमारे घर ऐसे काँप रहे थे जैसे हवा मेँ घास की पत्तियाँ। या हमारे इन घरों मेँ कैसी महामारियाँ
फैली हुई हैं।
तुम्हें इस सबकी कुछ खबर नहीं है। सब कुछ तुम्हें बताने मेँ पूरा दिन लग जाएगा। लोगों को सब्जियों और सभी प्रकार के सामानों के लिए लाइनों मेँ खड़े होना पड़ता है; डॉक्टर अपने मरीज़ोँ को नहीँ देख पाते ,क्योँकि उन्होँने पीठ मोड़ी नहीँ कि उनकी कारेँ और मोटर साइकिलेँ चुरा ली जाती हैँ ,चोरी -चकारी इतनी बढ़ गई है कि डच लोगोँ मेँ अँगूठी पहनने क रिवाज़ तक नहीँ रह गया है ।
छोटे-छोटे बच्चे आठ-आठ, दस-दस बरस के होंगे लेकिन लोगों के घरों की खिड़कियाँ तोड़ कर घुस जाते हैं और जो भी हाथ लगा, उठा ले जाते हैं। लोग पाँच मिनट के लिए भी अपना घर छोड़ने की हिम्मत नहीं कर सकते हैं, क्योँकि लौटने पर उन्हेँ घर में झाडू फिरी मिलेगी। चोरी गए टाइपराइटरों, ईरानी कालीनों, बिजली से चलने वाली घड़ियों, कपडों आदि को लौटाने के लिए अखबारों में इनाम के विज्ञापन आए दिन पढ़ने को मिलते हैं। गली-गली नुक्कडों पर लगी बिजली से चलने वाली घड़ियाँ लोग उतार ले गए और सार्वजनिक टेलीफ़ोनोँ का पुर्ज़ा-पुर्ज़ा गायब हो चुका है।
डचों की नैतिकता अच्छी नहीं है। सब भूखे हैं ; नकली कॉफ़ी को छोड़ दो तो एक हफ्ते का राशन दो दिन भी नहीं चल पाता। अभी और क्या देखना बाकी है, पुरुषों को जर्मनी
भेजा जा रहा है, बच्चे बीमार हैं या फिर भूख से बेहाल हैं; सब लोग फटे-पुराने कपड़े और घिसे-पिटे जूते पहनकर काम चला रहे हैं। ब्लैक मार्केट में जूते का नया तला 7.50 गिल्डर
का मिलता है। इसके अलावा बहूत कम मोची मरम्मत का काम कर रहे हैं, यदि वे करते
भी हैं तो चार महीने इंतजार करना महंगा और इस बीच जूता गायब हो चुका होगा।
इसका एक लाभ भी हुआ है, खाना जितना खराब होता जा रहा है बिक्री उतनी ही गंभीर
हो रही है; सरकारी लोगों पर हमले की घटनाएँ बढ़ती जा रही हैं। खाद्य कार्यालय, पुलिस, अधिकारी-सभी या तो अपने साथी नागरिकोँ की मदद कर रहे हैँ या उन पर कोई आरोप लगाकर जेल मेँ भेज देते हैँ । सौभाग्य से बहुत कम डच लोग गलत पक्ष मेँ हैँ ।
तुम्हारी ऐन
मंगलवार, 11 अप्रैल, 1944
मेरी प्यारी किट्टी,
मेरा सिर घूम रहा है। समझ में नहीं आ रहा , कहाँ से शुरू करू। गुरुवार (जब मैने
तुम्हें पिछली बार लिखा था) सब कुछ ठीक-ठाक था। शुक्रवार (गुड फ्राइडे) हम मोनापोली खेल खेलते रहे। शनिवार भी हम यही खेल खेले। दिन पता ही नहीं चला, कैसे बीत गए । शनिवार कोई दो बजे का वक्त रहा होगा, तेज़ गोलाबारी शुरू हो गई। मशीनगनें चल रही थीं। मर्द लोगोँ का यही कहना था । बाकी लोगोँ के लिए सब कुछ शांत था ।
रविवार दोपहर के वक्त मेरे आमन्त्रण पर पीटर साढ़े चार बज मुझसे मिलन के लिए
आया। सवा पाँच बजे हम ऊपर सामने वाली अटारी पर चले गए। वहाँ हम छ : बजे तक रहे। छ: बजे से सवा रात बजे तक रेडियों पर बहुत ही खूबसूरत मोत्ज़ार्ट संगीत बज रहा था। मुझे रात्रि राग बहुत ही भले लगे। मैं रसोई में तो संगीत खुन ही नहीं गाती, क्योँकि दिव्य
संगीत मेरी आत्मा की गहराइयों में उतरता चला जाता है। रविवार के दिन पीटर स्नान नहीं कर पाया था। नहाने का टब नीचे ऑफ़िस मेँ गंदे कपडों से भरा हुआ रखा था। हम दोनों ऊपर अटारी पर एक साथ गए। हम दोनों आराम से बैठ सकेँ, इसलिए मुझे जो भी कुशन सामने नज़र आया,
मैं ऊपर लेती गई। हम एक पेटी पर बैठ गए। अब हुआ यह कि एक तो वह पेटी बहुत छोटी थी और दूसरे कुशन भी छोटा-सा ही था, हम दोनों एक-दूसरे से बहुत सट कर बैठे हुए थे। सहारा लेने
के लिए हमारे पीछे दो और पेटियाँ थीँ ही। मोश्ची हमेँ कंपनी देने के लिए हमारे साथ थी ही।
अचानक पौने नौ बजे मिस्टर वान दान ने सीटी बजाई और पूछा कि कहीँ हम मिस्टर डसेल का कुशन तो नहीं ले आए हैं। हम कूदे और कुशन लेकर सीधे नीचे आ गए। बिल्ली और मिस्टर
वान दान हमारे साथ थे। यह कुशन ही सारे झगड़े की जड़ था। डसेल इसलिए खफ़ा थे कि मैं वो तकिया उठा लाई थी जिसे वे कुशन की तरह इस्तेमाल करते थे। उन्हेँ डर था कि उनके तकिए पर पिस्सु
चिपक जाएँगे। उन्होंने सारे घर को सिर पर उठा रखा था क्योँकि हम उनका कुशन उठा लाए थे। बदला लेने की नीयत से पीटर और मैंने उनके बिस्तर मेँ दो कड़े ब्रुश घुसेड़ दिए लेकिन जब मिस्टर डसेल
ने तय किया कि जाकर अपने कमरे मेँ बैठेँगे तो हमें ये ब्रुश निकाल लेने पड़े। इस छोटे से प्रहसन पर हम हँसते-हँसते लोट-पोट हो गए।
लेकिन हमारा हँसी-मज़ाक जल्दी ही खत्म हो गया। साढ़े-नौ बजे पीटर ने हौले से दरवाजा खटखटाया और पापा से कहा कि वे ज़रा ऊपर आएँ, उसे अंग्रेज़ी के एक कठिन वाक्य मेँ दिक्कत आ रही है।
मुझे तो दाल मेँ कुछ काला नज़र आ रहा है। 'मैँने मार्गोट से कहा, 'तय है, पीटर ने किसी और बहाने से यह बात कही है।' जिस तरीके से मर्द लोग बात कर रहे हैं, मैं शर्त लगा कर कह सकती हूँ कि सेंधमारी हो रही थी। पिता जी , मिस्टर वान दान औ रपीटर लपक कर नीचे पहुँच गए । मार्गोट , माँ , मिसेज़ वान दान और मैँ ऊपर इंतज़ार करते रहे । चार डरी-सहमी औरतेँ बातेँ ही तो कर सकती हैँ । जब तक हमने नीचे ज़ोर का एक धमाका नहीँ सुना ,हम बातोँ मेँ लगी रहीँ । उसके बाद का मामला है । मेरा सोचना सही था ।
उसी वक्त गोदाम में सब कुछ शांत हो गया। घड़ी ने पौने दस बजाए। हमारे चेहरों का रंग उड़ चुका था, इसके बावजूद कि हम डरे हुए थे, हम शांत बने रहे। आदमी लोग कहाँ थे? ये धमाके की आवाज कैसी थी ? क्या वे लोग सेंधमारोँ के साथ लड़ रहे थे? हम डर के मारे सोच भी नहीं पा रहे थे । हम सिर्फ़ इंतजार ही कर सकते थे।
दस बजे, सीढ़ियों पर कदमों की आवाजें आई। पापा का चेहरा पीला पड़ चुका था, वे
नर्वस थे। पहले वे भीतर आए। उनके पीछे मिस्टर वान दान, 'बत्तियाँ बंद कर दो, दबे पाँव
ऊपर वाली मंजिल पर चले जाओ, पुलिस के आने की आशंका है।'
अब डरने का वक्त भी नहीं बचा था। बत्तियाँ बुझा दी गईँ थीं। मैने फटाफट एक जैकेट उठाई और हम ऊपर जाकर बैठ गए। हमें कुछ भी बतानेचाला कोई भी नहीं था। मर्द लोग बापस नीचे जा चुके थे। वे चारों दस बज कर दस मिनट तक वापिस ही नहीं आए। दो लोग पीटर की खुली खिड़की में से निगाह रखे हुए थे। सीढियों के बीच वाले दरवाजे पर ताला जड़ दिया गया था। ब्रुककेस बंद कर दिया गया था। हमने रात को जलाई जाने वाली बत्ती
पर एक स्वेटर डाल दिया। तब उन्होंने हमें सब कुछ बताया कि क्या हुआ था।
पीटर अभी सीढ़ियों पर ही था जब उसने ज़ोर के दो धमाके सुने। वह नीचे गया तो
देखता क्या है कि गोदाम के दरवाजे में से बाईं तरफ़ का आधा फट्टा गायब है। वह लपक कर ऊपर आया और 'होम गार्डस' को चौकन्ना किया । वे चारोँ लपके-लपके नीचे गए । जब वे गोदाम मेँ पहुँचे तो सेंधमार अपने धंधे मेँ लगे हुए थे । बिना सोचे-समझे मिस्टर वान दान चिल्लाए,
'पुलिस…' बाहर भागने की आवाजें आईँ। सेँधमार भाग चुके थे । फट्टे को दोबारा
उसकी जगह पर लगाया गया ताकि पुलिस को इस गैप का पता न चले। लेकिन अभी एक
पल भी नहीं बीता था कि फट्टा फिर वापस नीचे गिरा दिया गया । पुरुष लोग...सेँधमारों की ढिठाई पर हैरान थे । मिस्टर वान दान और पीटर गुस्से के मारे थरथराने लगे । मिस्टर वान दान ने दरवाज़े
पर कुल्हाड़ी का एक ज़ोरदार प्रहार किया । उसके बाद सब कुछ शांत हो गया । एक बार फिर फट्टे को उसकी जगह पर जमाया गया और एक बार फिर उनका यह प्रयास निष्फल कर दिया गया । बाहर की तरफ़ से एक आदमी और एक औरत टॉर्च की रोशनी फेंकते दिखाई दिए। 'क्या मुसीबत है... ' उन आदमियों में से एक भुनभुनाया । लेकिन अब संकट यह था कि उनकी भूमिकाएँ बदल चुकी थीं । अब वे पुलिस के बजाए सेंधमारों वाली हालत में आ गए थे । चारों लपक कर ऊपर आए । डसेल और मिस्टर वान दान ने डसेल साहब की किताबेँ उठाईँ ,पीटर ने दरवाज़ा खोला , रसोई तथा प्राइवेट ऑफ़िस की खिड़कियाँ खोलीँ ।फ़ोन को नीचे फ़र्श पर पटका और आखिरकार चारोँ बुककेस के पीछे पहुँचने मेँ सफल हो ही गए ।
तुम्हारी ऐन
मंगलवार, 13 जून, 1944
मेरी प्यारी किट्टी,
मेरा एक और जन्मदिन गुज़र गया है। इस हिसाब से मैं
पंद्रह बरस की ही गई हूँ। मुझे काफ़ी सारे उपहार मिले हैं- स्प्रिँगर की पाँच खंडों वाली कलात्मक इतिहास पुस्तक, चड्ढियोँ का एक सेट, दो बेल्टेँ, एक रूमाल, दही के दो कटोरे, जैम की शीशी,
शहद वाले दो छोटे बिस्किट, मम्मी-पापा की तरफ़ से वनस्पति विज्ञान की एक किताब, मार्गोट की तरफ़ से सोने का एक ब्रेसलेट, वान दान परिवार की तरफ़ से स्टिकर एलबम, डसेल की तरफ़ से बायोमाल्ट और मीठे मटर, मिएप की तरफ़ से मिठाई, बेप की तरफ़ से मिठाई और लिखने के लिए कॉपियाँ और सबसे बड़ी बात मिस्टर कुगलर की तरफ़ से मारिया तेरेसा नाम की किताब तथा क्रीम से भरे
चीज़ के तीन स्लाइस । पीटर ने पीओनी फूलों का खूबसूरत गुलदस्ता दिया। बेचारे को ये उपहार जुटाने मेँ ही अच्छी खासी मेहनत करनी पड़ी। लेकिन वह कुछ और जुटा ही नहीं पाया।
बेहद खराब मौसम-लगातार बारिश, हवाएँ, और उफ़ान पर समुद्र के बावजूद हमले शानदार तरीके से जारी हैं।
कल चर्चिल, स्मट्स, आइज़नहावर, तथा आर्मोल्ड उन फ्रांसीसी गाँवोँ मेँ गए जिन पर ब्रिटिश सैनिकों ने पहले कब्जा कर लिया था
और बाद मेँ मुक्त कर दिया। चर्चिल एक टॉरपीडो नाव मेँ थे। इससे तटों पर गोलाबारी की जाती है। बहुत से लोगों की तरह चर्चिल को भी पता नहीं है-डर किस चिड़िया का नाम है। जन्मजात बहादुर ।
यहाँ हमारी एनेक्सी की किलेबंदी से डच लोगों के मूड की थाह पाना बहुत मुश्किल है । इस बात मेँ कोई शक नहीँ कि लोगबाग बैठे ठाले भी खुश रह लेते हैँ । ब्रिटिश सैनिकोँ ने आखिर अपनी कमर कस ही ली है और अपने मकसद को पूरा करने के लिए निकल पड़े हैँ । जो लोग ये दावे करते फिर रहे हैँ कि वे ब्रिटिश द्वारा कब्ज़ा किए जाने के पक्ष मेँ नहीँ हैँ , नहीँ जानते कि वे कितनी गलती पर हैँ । उनके तर्क का कारण इतना भर है -ब्रिटिश को लड़ते रहना चाहिए ,संघर्ष करना चाहिए ,और हॉलैँड को आज़ाद कराने के लिए अपने शूरवीर सैनिकों की शहादत के लिए आगे आना चाहिए। हॉलैंड के साथ-साथ कब्जे वाले दूसरे देशों को भी आजाद कराना चाहिए, लेकिन उसके बाद ब्रिटिश को हॉलैंड में रुकना नहीं चाहिए। इसके बजाय उन्हेँ चाहिए कि वे सभी कब्ज़े वाले देशों से हाथ जोड़-जोड़कर माफी माँगें, डच ईस्ट इंडीज को उसके सही हकदारों के हाथोँ में सौंपे और थके, टूटे, हारे और लुटे-पिटे अपने देश ब्रिटेन में लौट जाएँ। मूर्खोँ की कहीं कोई कमी नहीं है। इसके बावजूद, जैसा कि मैने कहा, कुछेक समझदार डच लोगों की भी कमी नहीं है। अगर ब्रिटिश ने जर्मनी के साथ शांति संधि पर हस्ताक्षर कर लिए होते तो हॉलैंड और उसके पड़ोसी देशों का क्या हाल हुआ होता। उसके पास ऐसा करने के बहुत मौके मौजूद थे। हॉलैँड जर्मनी बन चुका होता और तब-यह होना ही समाप्ति का संकेत होता। सब कुछ खत्म हो जाने का संकेत ।
ऐसे सभी डच लोग, जो अभी भी ब्रिटिश को हिकारत से देखते हैं, ब्रिटेन की खिल्ली
उड़ाते हैं, उसके बुढ़ाते लॉर्डोँ की सरकार को ताने मारते हैं, उन्हें कायर कहते हैं, इसके बावजूद जर्मनों से नफ़रत करते हैं, एक अच्छा-खासा सिखाने के लायक हैँ । उनकी जमकर मरम्त की जानी चाहिए तभी हमारे जंग लगे दिमाग खुलेँगे । उनमेँ जोश आएगा ।
मेरे दिमाग में हर समय इच्छाएँ, विचार, आरोप तथा डाँट-फटकार ही चक्कर खाते रहते हैं। मैं सचमुच उतनी घमंडी नहीं हूँ जितना लोग मुझे समझते हैं। मैँ किसी और की तुलना में अपनी कई कमजोरियों और खामियों को बेहतर तरीके से जानती हूँ। लेकिन एक फ़र्क है-मैँ जानती हूँ कि मैँ खुद को बदलना चाहती हूँ, बदलूँगी और काफ़ी हद तक बदल चुकी हूँ।
तब ऐसा क्यों है, मैं अपने आप से यह सवाल पूछती हूँ कि लोग मुझे अभी भी इतना
नाक घुसेड़ू और अपने आपकी तीसमारखाँ समझने वाली क्यों मानते हैं? क्या मैँ वाकई
अक्खड़ हूँ ? क्या मैँ ही अकेली अक्खड़ हूँ या वे सब ही हैं? यह सब वाहियात लगता है, मुझे पता है। लेकिन मैं ऊपर लिखा ये आखिरी वाक्य काटने वाली नहीं। ये वाक्य इतना
मूर्खतापूर्ण नहीं है जितना लगता है। मुझ पर हमेशा आरोपों की बौछार करते रहने वाले दो लोग है मिसेज वान दान और डसेल, उनके बारे में सबको पता है कि वे कितने जड़बुद्धि हैँ । मूर्ख जिसके आगे कोई विशेषण लगाने की ज़रूरत नहीँ । मूर्ख लोग आमतौर पर इस बात को सहन नहीँ कर पाते कि कोई उनसे बेहतर काम करके दिखाए । और इसका सबसे बढ़िया उदाहरण ये दो ज़ड़मति, मिसेज़ वान दान और मूर्खाधिराज डसेल हैँ। मिसेज़ वान दान मुझे
इसलिए मूर्ख समझती हैँ क्योँकि मैं उनके जितनी बीमारियों की शिकार नहीं हूँ। वे मुझे अक्खड़ समझती है क्योँकि वे मुझसे भी ज्यादा अक्खड़ हैं। वे समझती है कि मेरी पोशाकेँ छोटी पड़ गई हैं, क्योंकि उनकी पोशाकें और भी ज्यादा छोटी पड़ गई हैं। और वे समझती कि मैं अपने अपाको कुछ ज्यादा ही तीसमारखाँ समझती हूँ क्योँकि वे उन विषयों पर मुझसे भी दो गुना ज्यादा बोलती हैं जिनके बारे मेँ वे खाक भी नहीं जानतीं। यह बात डसेल पर भी फिट होती है। लेकिन मेरी प्रिय
कहावत है-"जहाँ आग होगी, धुआँ भी वहीं होगा'। और मुझे यह मानने मेँ रत्ती-भर भी संकोच नहीं है कि मैं सब कुछ जानती हूँ।
मेरे व्यक्तित्व के साथ सबसे मुश्किल बात यह है कि मैं
किसी भी और व्यक्ति की तुलना मेँ अपने आपको सबसे
धिक्कारती हूँ , यदि माँ अपनी सलाहें देना शुरू कर देती हैं तो उनके उपदेशों की पोटली इतनी भारी हो जाती है कि मुझे डर लगने लगता है- कैसे होगी इससे मुक्ति! जब तक ऐन का वही पुराना रूप सामने नहीं आ जाता-'मुझे कोई नहीं समझता।'
यह वाक्य मेरा हिस्सा है। बेशक लगे कि ऐसा नहीं होगा,
फिर भी इसमें थोड़े से सच का अंश है। कई बार तो मैं अपने
आपको प्रताडित करते हुए इतनी गहरे उतर जाती हूँ कि सांत्वना के दो बोल सुनने के लिए तरस जाती हूँ कि कोई आए और मुझे इससे उबारे। काश, कोई तो होता जो मेरी भावनाओँ को गंभीरता से समझ पाता। अफ़सोस, ऐसा व्यक्ति मुझे अब तक नहीं मिला है, इसलिए तलाश जारी रहेगी।
मुझे पता है, तुम पीटर के बारे मेँ सोचकर हैरान हो रही ही। नहीं क्या, किट्टी? मैं मानती हूँ कि यह सच है कि पीटर मुझे प्यार करता है गर्लफ्रेंड की तरह नहीं बल्कि एक दोस्त की तरह । उसका स्नेह दिन पर दिन बढ़ता ही जा रहा है; लेकिन कई बार
कोई रहस्यमयी ताकत हम दोनों को पीछे की तरफ़ खींचती है। मैं नहीं जानती कि वो कौन-सी शक्ति है।
कई बार मैं सोचती हूँ कि मैं उसके पीछे जिस तरह
प्रेमदीवानी बनी रहती हूँ, उसे बढ़ा-चढ़ाकर बता रही हूँ, लेकिन यह सच नहीं है। इसका कारण यह है कि अगर मैं उसके कमरे मेँ एक-दो दिन के लिए न जा पाऊं तो मेरी बुरी हालत हो जाती है। मैं उसके लिए तड़पऩे लगती हूँ। पीटर अच्छा और भला लड़का है ; लेकिन उसने मुझे कई तरह से निराश किया है । धर्म के प्रति उसकी नफ़रत ,खाने के बारे मेँ उसका बातेँ करना और इस तरह की और कई बातेँ मैँ बिलकुल भी पसंद नहीँ करती । इसके बावजूद मुझे पक्का यकीन है कि हमने जो वायदा किया है कि कभी झगड़ेगे नहीं, हम उस
पर हमेशा टिके रहेंगे। पीटर शांतिप्रिय, सहनशील और बेहद सहज आत्मीय व्यक्ति है। वह मुझे कई ऐसी बातें भी कह लेने देता है जिन्हेँ कहने की वह अपनी मम्मी को भी इजाज़त न देता। वह दृढ निश्चयी होकर इस मुहिम पर जुटा हुआ है कि वह अपने पर लगे हुए सभी इल्ज़ामों से अपने आपको पाक-साफ़ करें और अपने काम-काज़ में सलीका लाए। इसके बावजूद वह अपने भीतरी 'स्व' को मुझसे छुपाता क्योँ है और मुझे कभी भी इस बात की अनुमति नहीं देता कि मैँ उसमें झाँकूँ। निश्चय ही, वह मेरी तुलना में ज्यादा घुन्ना है, लेकिन
मैँ अनुभव से जानती हूँ (हालँकि मुझ पर लगातार यह आरोप लगाया जाता है कि जो कुछ भी जानना चाहिए वह मैँ थ्योरी में जानती हूँ, व्यवहार में नहीं) कि कई बार, ऐसे घुन्ने लोग भी, जिनसे संवाद कर पाना बहूत मुश्किल होता है, अपनी बात किसी से कह पाने की उत्कट चाह लिए होते हैं।
पीटर और मैँने, दोनों ने अपने चिंतनशील बस्स, एनेक्सी में ही बिताए हैं। हम अकसर
भविष्य, वर्तमान और अतीत की बातें करते हैं, लेकिन जैसा कि मैं तुम्हें बता चुकी हूँ, मैँ
असली चीज की कमी महसूस करती हूँ और जानती हूँ कि वह मौजूद है।
क्या इसका कारण यह है कि मैँ अरसे से बाहर नहीं निकली हूँ और प्रकृति के लिए
पागल हुई जा रही हूँ। मैं उस वक्त को याद करती हूँ जब नीला आसमान , पक्षियोँ की चहचहाने की आवाज़ , चाँदनी और खिलती कलियाँ ,इन चीज़ोँ ने मुझे कभी भी अपने जादू से बाँधा न होता। मेरे यहाँ आने के बाद चीज़ेँ बदल गई हैं। उदाहरण के लिए छुट्टियों के दौरान की बात है। बेहद गरमी थी। मैं रात के साढ़े ग्यारह बजे तक जबरदस्ती आँखें खोले बैठी रही ताकि मैं अपने अकेले के बूते पर अच्छी तरह चाँद को देख सकूँ । अफ़सोस, मेरी
सारी मेहनत बेकार गई। चौंध इतनी ज्यादा थी कि खिड़की खेलने का जोखिम नहीं लिया जा सकता था। कई महीने बाद एक और मौका ऐसा आया था। उस रात मैं ऊपर वाली मंजिल पर थी। खिड़की खुली हुई थी। जब तक खिड़की बंद करने का वक्त नहीं हो गया है मैँ वहीं बैठी रही। यह गहरी, साँवली बरसात की रात थी। तेज हवाएँ चल रही थीं। बादलों के बीच लुकाछिपी चल रही थी। इस सारे नज़ारे ने मुझे मंत्रमुग्ध कर दिया था। पिछले डेढ़ बरस में पहली बार हो रहा था कि मैँ आमने-सामने रात से साक्षात्कार कर रही थी। उम शाम के बाद प्रकृति से साक्षात्कार करने की मेरी चाह लगातार बढ़ती गई थी । तब मुझे चोर उचक्कोँ , मोटे काले चूहे या पुलिस के छापे का भी डर नहीँ रहा था । मैं अकेले ही नीचे चली गई थी और रसोई तथा प्राइवेट ऑफ़िस की खिड़की से प्रकृति के नज़ारे देखती रही
थी । कई लोग सोचते हैँ कि प्रकृति सुंदर होती है, कई लोग समय-समय पर तारों भरे
आसमान के तले सोते हैं,और कई लोग अस्पतालों और जेलों में उस दिन की राह देखते रहते हैं कि वे कब आजाद होंगे और वे फिर से प्रकृति के इस अनूठे उपहार का आनंद ले पाएँगे। प्रकृति गरीब-अमीर के बीच कोई भेदभाव नहीं करती।
यह मेरी कल्पना मात्र नहीं है-आसमान, बादलों, चाँद और
तारों की तरफ़ देखना मुझे शांति और आशा की भावना से सराबोर कर देता है। यह वेलेरियन या ब्रोमाइड की तुलना मेँ आजमाया हुआ
बेहतर नुस्खा है। शांति पाने की रामबाण दबा। प्रकृति मुझे विनम्रता का उपहार देती है और इससे मैं बड़े से बड़ा धक्का भी हिम्मत के साथ झेल जाती हूँ। लेकिन किस्मत का लिखा यही है-कुछेक दुर्लभ अवसरों को छोड़कर मैं मैल से चीकट हुई खिड़कियोँ मेँ खुँसे गंदे परदों मेँ से प्रकृति को बहुत ही कम निहार पाती हूँ। इस तरह से देखने से आनंद लेने की सारी भावना ही मर जाती है। प्रकृति ही तो एक ऐसा वरदान है जिसका कोई सानी नहीं।
कई प्रश्नों मेँ से एक प्रश्न जो मुझे अकसर परेशान करता
रहता है और अभी भी समझा जाता है यह कह देना वहुत ही आसान है कि ये गलत है, लेकिन मेरे लिए इतना ही काफ़ी नहीं है। मैं इस
विराट अन्याय के कारण जानना चाहती हूँ।
संभवत: पुरुषों ने औरतों पर शुरू से ही इस आधार पर शासन करना शुरू किया कि वे उनकी तुलना मेँ शारीरिक रूप से ज्यादा सक्षम हैं; पुरुष ही कमाकर लाता है; बच्चे पालता पोसता है; और जो मन मेँ आए, करता है, लेकिन हाल ही मेँ स्थिति बदली है।
औरतें अब तक इन सबको सहती चली आ रही थीं, जो कि बेवकूफ़ी ही थी। चूँकि इस प्रथा को जितना अधिक जारी रखा गया, यह उतनी ही गहराई से अपनी जड़ेँ जमाती चली गई । सौभाग्य से , शिक्षा ,काम तथा प्रगति ने औरतोँ की आँखेँ खोली हैँ । कई देशोँ मेँ तो उन्हेँ बराबरी का हक दिया जाने लगा है । कई लोगोँ ने कई औरतोँ ने और कुछेक पुरुषोँ ने भी अब इस बात को महसूस किया है कि इतने लंबे अरसे तक इस तरह की वाहियात स्थिति को झेलते जाना गलत ही था । आधुनिक महिलाएँ पूरी तरह स्वतंत्र होने का हक चाहती हैँ ।
लेकिन इतना ही काफ़ी नहीं है। महिलाओँ का भी पूरा सम्मान किया जाना चाहिए।
आमतौर पर देखा जाए तो पूरी दुनिया में पुरुष वर्ग को पूरा सम्मान मिलता है तो महिलाओँ ने ही क्या कुसूर किया है कि वे इससे वंचित रहेँ और उन्हेँ अपने हिस्से का सम्मान न मिले। सैनिकों और युद्धों के वीरों का सम्मान किया जाता है, उन्हेँ अलंकृत किया जाता है, उन्हेँ अमर बना डालने तक का शौर्य प्रदान किया जाता है, शहीदों को पूजा भी जाता है, लेकिन
कितने लोग ऐसे हैं जो औरतों को भी सैनिक का दर्जा देते हैं?
'मौत के खिलाफ़ मनुष्य' नाम की किताब में मैंने पढ़ा था कि आमतौर पर युद्ध में लड़ने वाले वीर को जितनी तकलीफ़, पीड़ा, बीमारी और यंत्रणा से गुज़रना पड़ता है, उससे कहीं अधिक तकलीफ़ेँ औरतें बच्चे को जन्म देते समय झेलती हैं और इन सारी तकलीफ़ोँ से गुज़रने के बाद उसे पुरस्कार क्या मिलता है? जब बच्चा जनने के बाद उसका शरीर अपना आकर्षण खो देता है तो उसे एक तरफ़ धकिया दिया जाता है, उसके बच्चे उसे छोड़
देते हैं और उसका सौँदर्य उससे विदा ले लेता है। औरत ही तो है जो मानव जाति की
निरंतरता को बनाए रखने के लिए इतनी तकलीफ़ोँ से गुज़रती है और संघर्ष करती है, बहुत अधिक मज़बूत और बहादुर सिपाहियों से भी ज्यादा मेहनत करके खटती है। वह जितना संघर्ष करती है, उतना तो बड़ी-बड़ी डीँगेँ हाँकनेवाले ये सारे सिपाही मिलकर भी नही करते ।
मेरा ये कहने का कतई मतलब नहीं है कि औरतों को बच्चे जनना बंद कर देना चाहिए , इसके विपरीत प्रकृति चाहती है कि वे ऐसा करें और इस वजह से उन्हेँ यह काम करते रहना चाहिए। मैं जिस चीज की भर्त्सना करती हूँ वह है हमारे मूल्यों की प्रथा और ऐसे व्यक्तियों की मैँ भर्त्सना करती हूँ जो यह बात मानने को तैयार ही नहीं होते कि समाज में औरतों, खूबसूरत और सौँदर्यमयी औरतों का योगदान कितना महान और मुश्किल है।
मैं इस पुस्तक के लेखक श्री पोल दे क्रुइफ जी से पूरी तरह सहमत हूँ जब वे कहते है कि पुरुषों को यह बात सीखनी ही चाहिए कि संसार के जिन हिस्सों को हम सभ्य कहते
हैं-वहाँ जन्म अनिवार्य और टाला न जा सकने वाला काम नहीं रह गया है। आदमियों के
लिए बात करना वहुत आसान होता है-उन्हेँ औरतों द्वारा झेली जाने वाली तकलीफ़ो से कभी भी गुजरना नहीं पड़ेगा।
मेरा विश्वास है कि अगली सदी आने तक यह मान्यता बदल चुकी होगी कि बच्चे पैदा करना ही औरतोँ का काम है । औरतेँ ज़्यादा सम्मान और सराहना की हकदार बनेँगी ।वे सब औरतेँ जो एक उफ़ भी किए बिना ,यह लंबे-चौड़े बखानोँ के बिना ये तकलीफ़ेँ सहती हैँ ।
तुम्हारी
ऐन.एम.फ्रैँक
-अनुवाद : सूरज प्रकाश